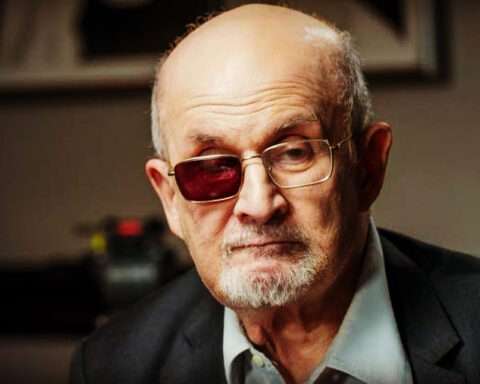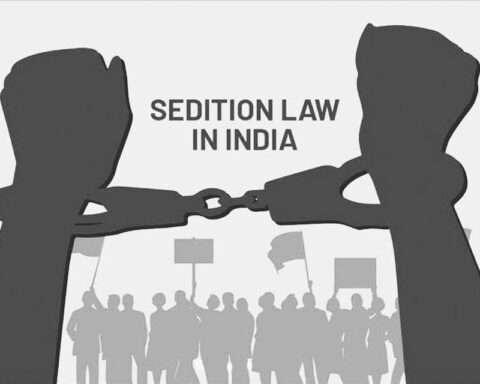(रानीखेत; जुलाई, 1975)
कहते हैं, आदमी को पूरी निर्ममता से अपने अतीत में किये कार्यों की चीर-फाड़ करनी चाहिए, ताकि वह इतना साहस जुटा सके कि हर दिन थोड़ा-सा जी सके। लेकिन जब वह अपने अतीत को देखता है, तो एक अँधेरी सुरंग में चला जाता है, हर कदम किसी पाप, और फिर उससे भी बड़े पाप की ओर बढ़ता हुआ। प्रलोभन और अभिमान (लोभ और अहंकार) का पाप, जीवन से अधिक और जीने की वासना का पाप, सैकड़ों वासनाएँ आग की लपट पर मँडराती हुई, एक-एक पतिंगे की तरह जलती हुई।
लेकिन सब नहीं – कुछ वासनाएँ लौ के ऊपर अपने एकान्त में झुलसती रहती हैं जबकि वह उनके मरने की प्रतीक्षा और प्रार्थना करता रहता है। उनके मरण की प्रतीक्षा करता हुआ लेकिन उनकी राख में स्वयं को मिटाने की प्रार्थना करता हुआ, ताकि यह उसमें से अपनी खोई हुई पवित्रता को प्राप्त कर सके…यह कैसा अन्तर्विरोध है, वह अपनी पवित्रता को उन्हीं वासनाओं की राख से पुनर्जीवित करना चाहता है, जिन्हें वह छोड़ना नहीं चाहता या शायद चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पाता।
रिल्के की ये पंक्तियाँ कहीं पिछले वर्षों की मेरी मनोदशा को प्रकट करती है-
मेरा आन्तरिक जीवन पिछले महीनों में अव्यवस्थित हो गया है,
और मेरा मौजूदा अकेलापन एक तरह से मेरे मन पर बंधी प्लास्टर पट्टी है,
जिसके भीतर कुछ धीरे-धीरे तिरोहित हो रहा है।
मैंने जो व्यवसाय चुना है, उससे ज्यादा ईर्ष्यालु शायद कोई और चीज़ नहीं। यह जानते हुए भी कि मेरी कोई भिक्षुक की ज़िन्दगी नहीं है, जो मोनेस्ट्री की कोठरी में सारी दुनिया से अलग-थलग रहता है, मुझे धीरे-धीरे अपने इर्द-गिर्द एक मोनेस्ट्री बनानी चाहिए ताकि मैं दीवारों से घिरा हुआ दुनिया के सामने खड़ा हो सकूँ,सिर्फ़ ईश्वर और सन्त मेरे भीतर हों, बहुत सुन्दर औजारों और प्रतिमाओं के साथ …
स्तान्ढाल की पुस्तक ब्रूनार्ड की ज़िन्दगी पढ़ते हुए मुझे एक बहुत सजीव अनुभूति हुई मानो मैं एक पहाड़ी झरने का साफ, शीतल जल पी रहा हूँ। शायद सब सरल और गहरे सत्य यही अनुभूति देते हैं और यह पुस्तक इन सत्यों का प्रत्यक्षीकरण, ‘क्रिस्टलन‘ है।
शाम को जब हवा का वेग बढ़ता है और चीड़ की टहनियाँ पागलों-सी डोलती हैं-मैं अपने से नितान्त निस्संग हो जाता हूँ और अपने को बाहर की शक्तियों के प्रति समर्पित कर देता हूँ – हिलते हए वृक्ष, तारे, भुतैली-सी चाँदनी चीड़ों पर चमकती हुई — और तब किसी विराट बोध के समक्ष मेरा दिल सिहरने लगता है, जो आख़िरी क्षण मेरे हाथों से फिसल जाता है, जैसे ही मुझे लगता है कि मैंने उसे पा लिया है। मैंने कभी ईश्वर में विश्वास नहीं किया, किन्तु इन दिनों, ख़ासकर रात के समय, जब चाँद निकलता है, मैं अपने को उसके बहुत निकट पाता हूँ, ईश्वर के नहीं बल्कि उस ‘रहस्य‘ के जो उसके नाम के चारों ओर फैला है, जिसके साथ मेरा हर रोज़ साक्षात्कार होता है, सूरज और बादलों में, पेड़ और चाँद जो बादलों के ‘कुशन पर थिर रहते हैं और बादल तारों के बीच तिरते जाते हैं, उस पपड़ी को धो डालते हैं, जो मेरी आत्मा पर जम गयी थी और एक बार धुलने के बाद वह अपने में लपेट लेता है — मुझे नहीं, मेरे दिल और भावनाओं को नहीं, लेकिन उसे जो मुझे आवृत्त किये रहता है – मेरे नंगे नैसर्गिक जीवत्व को।
कुछ दिन पहले मैं अचानक अर्द्धरात्रि में जाग गया, बाहर बरामदे में आया, जो ‘एटिक‘ से जुड़ा है, जहाँ मैं पहले सोया करता था। वहाँ खड़े होकर मैं चीड़ को देखने लगा, जिनकी कटी-छँटी रूपरेखा अँधेरे में एक चित्र-सी खिंची थी। गहरी निस्तब्धता। मैं अपनी साँसें सुन सकता था। हवा नहीं थी, चाँद भी नहीं। सिर्फ तारे और निस्तब्धता-और पेड़ निश्चल खड़े थे, एक-दूसरे से सटे हुए, उनकी फुनगियाँ तारों को छूती हुई। सबसे विस्मयकारी बात यह थी कि जब वे अपने में लिपटे, स्थिर थे, शान्त और आत्म-अन्तनिष्ट, मैंने अपने को उनके बीच अनामन्त्रित नहीं पाया, कोई बाहर का दर्शक नहीं, बल्कि हमेशा उनके साथ रहने वाला जीव, उतना ही अलग-थलग और अकेला जितना वे थे, किन्तु अपने अकेलेपन में उनसे अलग नहीं। उनके सान्निध्य में ही मैंने सीखा था कि अपने एकांत में रहकर भी पीड़ा मुक्त रहा जा सकता है। मैंने देखा, अपनी शान्त निश्चलता में वे कितने भव्य, ग्रेसफल और शक्तिमान दिखाई देते हैं, शायद इसलिए कि वे अपने ‘ग्रहपथ‘ से इतनी गहराई से जुड़े हैं, आकाश के नक्षत्र, धरती में धंसे वृक्ष। उनकी यह बद्धमूलता ही है जो इनके और हमारे अकेलेपन को इतनी गरिमा देती है।
किन्तु ईश्वर अगर फूल और वृक्ष है।
पहाड़ियाँ, सूरज और चाँदनी,
तब मैं उसमें विश्वास करता हूँ।
तब मैं हर घड़ी उसमें विश्वास करता हूँ
तब मेरा समूचा जीवन एक प्रार्थना और यज्ञ है
आँखों और कानों में रचता एक समागम।
–पेसोआ
ये पत्र कहीं परोक्ष रूप से लिखने के साथ भी जुड़े हैं … इन दिनों मैंने अपने बारे में यह परम सत्य पाया है, कि मेरा अकेलापन वह यथार्थ है, जो ‘फैन्टेसी‘ को रूपायित करेगा, सिर्फ़ उसे फॉर्म नहीं देगा, बल्कि उसकी त्वचा नीचे अर्थ को खोजेगा, जो सिर्फ़ मेरा है और जिसे मैं ‘यज्ञाहुति‘ की तरह उस पर चढ़ा सकूँगा, जो मैंने सृजित किया है, अर्थ जो चढ़ाया हुआ भोग भी है बचा हुआ प्रसाद भी।

निर्मल वर्मा
निर्मल वर्मा (03/04/1929 – 25/10/2005) हिंदी के मूर्धन्य कथाकार और पत्रकार रहे. उन्हें ‘नयी कहानी साहित्यिक आन्दोलन’ के लिए भी श्रेय दिया जाता है. उन्हें 1985 में साहित्य अकादमी, 1999 में ज्ञानपीठ और 2002 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया. उन्हें ‘परिंदे’ और ‘अंतिम अरण्य’ जैसी कृतियों के लिए याद किया जाता है.