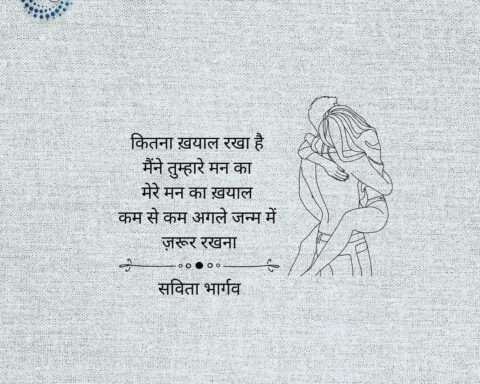एक निजी कथन से अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ। मैं कवि हूँ, लेकिन हर समय नहीं। स्वतंत्र भी मैं उतनी ही हूँ जितना अपने को होने देती हूँ। लेकिन स्त्री हूँ, इसका बोध मुझे सोते-जागते हर क्षण रहता है। कपड़ों के चुनाव में, उठने-बैठने के ढंग में, बोलचाल की भाषा में कौन-से शब्द मेरे मुँह पर न आएँ – इसमें। ये तीनों भाव मेरे होने को अपनी-अपनी तरह गढ़ते हैं, लुकन-छिपी खेलते हैं, कभी मेरी कविता पकड़ में आ जाती, कभी मेरी स्वतंत्रता और कभी मेरी स्त्री।
लिखने का क्षण जितना कष्टकर बन कर आता है, उसके चलते कई बार इच्छा हुई है कि इस समय मैं कवि होने की बजाय कुछ भी और हो सकूँ तो कितना अच्छा हो। घर के किसी पौधे का पीला पत्ता हटा दूँ। गिलास कमरे से उठाकर सिंक में रख आऊँ। चादर की सिलवट ठीक कर दूँ। वह क्षण आता है तो कहीं नीचे पसलियों में साँस अटक जाती है, अँधेरा घिरने लगता है, आसपास की आवाजें कहीं और जाने लगती हैं। महादेवी अक्का के शब्दों में कहें तो ‘जैसे रेशम का कीड़ा बुनता है अपना घर’। कोरे कागज पर एक शब्द लिखा जाता है, कभी एक पूरी पंक्ति। उस सारी शारीरिक यातना का ‘निचोड़’ – सिर्फ यह। समूची कविता मालूम नहीं कब बनती है, कैसे बनती है। और जो कविता, अंतिम ड्राफ्ट में छपने के लिए तैयार होती है, उसमें इस प्रथम त्रासदायी क्षण की स्मृति हो ही – यह जरूरी नहीं।
कितना अच्छा है कि मैं हर समय कवि नहीं हूँ। एलेन सिक्सू ने जिसे ‘born carried away’ कहा है, वह नहीं हूँ। यदि मैं वह होती तो मेरी मानसिक हालत को खतरा हो सकता था। एड्रियन रिच की वह स्त्री भी मैं नहीं हूँ, जिसके लिए उन्होंने कहा है, वह स्त्री उठाए है मेरा उन्माद और मुझे उससे डर लगता है। ‘She is carrying my madness and I dread her.’ मेरी यह काया, यह व्यक्ति-विशेष मुझे कभी-कभार पागलपन के पानियों में डूबने-उतरने की मोहलत देते हैं और समय रहते बाहर निकाल लेते हैं। किसी अच्छे दिन मैं किसी बनी-अधबनी कविता का मोती चुग आती हूँ। क्या यह सौभाग्य नहीं? जो लोग मुंडेरों पर झूलते रहते हैं, उनमें से कितनों को बचने का यह मौका मिलता है?
कितना अच्छा है कि मैं पूरी तरह स्वतंत्र भी नहीं हूँ। स्व के बनाए तंत्र में, तंतु जाल में कितने ही बारीक गड़हे हैं, हो सकते हैं। उनमें किसी में भी गलत जगह मेरा पैर पड़ सकता है। परंपरा द्वारा परिभाषित और रेखांकित मेरी स्त्री भले ही कभी-कभी मुझे कुंठित करती हो, लेकिन वही मेरा आसरा बनती है। कविता और स्वतंत्रता की माँगों से थक कर जब मैं उसके कंधे पर अपना सिर टिकाती हूँ, वह मेरे लिए एक अदृश्य द्वार खोलती है – समस्त स्त्रियों के एकांत का प्रवेश-द्वार। यहीं मैं वह होती हूँ, जिसे होने के लिए मुझे प्रयास नहीं करना पड़ता। संसार से छिटक कर मैं अपनी नाभि से जुड़ती हूँ।
###
क्या है एक स्त्री का एकांत? वह एक पुरुष के, एक जाति के, एक आदिवासी के एकांत से किस तरह भिन्न है? स्त्रियों के एकांत में देवता नहीं रहते। ईश्वर नहीं रहता। उसमें भवसागर है और भवबाधाएँ। कुछ प्राचीन कथाएँ हैं और स्वप्न। और धुँधली-सी एक धुन, जिसे वे हर देश-काल में अपनी-अपनी तरह से पकड़ती हैं। इस धुन को पकाते हुए ही वे अपनी काया से बाहर आती हैं काल की गिरफ्त से स्वतंत्र होती हैं। लेखन अंततः एक तरह का शव-आसन ही है। अपने शरीर, अपनी काया से बाहर खड़े होकर अपना होना देखना। एक प्रकार की सिद्धि, जो हमारे यहाँ सैकड़ों वर्षों से योगी करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अपने स्त्रीत्व को पार करने के बाद एक स्त्री अंत में जिसे हासिल करती है वह इस पृथ्वी पर अपने होने के बारे में ही एक नई-साफ समझ है। देह, एक स्त्री-देह, इस सब को जानने हेतु ज्यादा से ज्यादा एक औजार भर है, स्टैथोस्कोप के सिरे पर लगा एक काँच। उसके भीतर जो सुनाई पड़ता है, वह जितना औजार के कारण है, उतना ही उस ‘उपस्थिति’ के कारण, जिसे वह एक क्षण-विशेष में एक विशेष दबाव से छूती है।
ठिठक गई मैं
पेड़ के पास
हवा
डाल पकड़ कर झूल रही थी
हवा में
(ज्योत्स्ना मिलन : ‘हवा : पेड़’)
हवा डाल पकड़ कर झूल रही है, दर्ज करने के लिए जरूरी है कि न सिर्फ कोई ‘मैं’ वहाँ से गुजरे, बल्कि ठिठक भी जाए। ठिठकना ही इस सृष्टि को देखना है – ईश्वर की कोमल स्त्री-दृष्टि से देखना। एक व्यापक अर्थ में सारे का सारा स्त्री-लेखन उन जगहों पर ठिठक कर देखने का क्षण है, जहाँ ‘पुरुष-लेखक’ तो क्या, शायद ईश्वर भी स्थितियों की साधारणता, अनाटकीयता के कारण नहीं रुकता। सृष्टि अपने कुछ रहस्य एक स्त्री-दृष्टि की प्रत्याशा में छिपाए रखती है, कुछ वैसे ही जैसे एक पौरुष की आकांक्षा में वह नित्य नए महा-सत्य प्रस्तुत करती है।
यहाँ मैं स्त्री दृष्टि की बात कर रही हूँ। स्त्री की दृष्टि की नहीं। जरूरी नहीं कि एक स्त्री के पास स्त्री दृष्टि हो ही। बल्कि हममें से अधिकांश तो स्वयं को, स्वयं की दुनिया को, एक मानक पुरुष दृष्टि से देखने की इतनी सहज अभ्यस्त हैं कि किसी भी दूसरी तरह से स्वयं को देख पाना हमारे लिए मुश्किल होगा। विडंबना तो यह है कि हमारे यहाँ का अधिकांश स्त्री-लेखन स्वयं को इसी पुरुष-दृष्टि से परखने का लेखन है। इसीलिए वह कमतर भी है। जहाँ-जहाँ स्त्री ने स्वयं को स्वयं की दृष्टि से देखा है, वह अपने वर्ण-वर्ग से परे चली आई है। अपनी जाति से मुक्त हो गई है। यदि आज तथाकथित ‘पुरुष’ लेखन ही मुख्यधारा साहित्य माना जा रहा है तो इसलिए भी कि अपने सृजन-कर्म में पुरुष सहज है, उसके मन में अपनी जाति के कारण या इस सृष्टि में अपनी जगह को लेकर कोई फाँक नहीं है। उसके सब रचनात्मक संकटों में उसके पैरों के नीचे एक पुख्ता जमीन है और स्त्री की जमीन? और एक दलित की जमीन, एक अप्रवासी की जमीन, एक अश्वेत की जमीन? वह बार-बार हिलती है। हिलती है और उसमें से खाँचे निकलते आते हैं – स्त्री-लेखन, दलित-लेखन, अप्रवासी-लेखन, अश्वेत-लेखन…
एक स्त्री के यहाँ घर प्रायः एक स्वप्न है, संतान एक स्वप्न है, प्रेम तो ख़ैर स्वप्न है ही। जितना अधिक एक स्त्री यथार्थ में इनसे घिरती जाती है, उतना वे सब उसकी कल्पना में अमूर्त होते जाते हैं। बल्कि कुछ ऐसे कि कल्पना का घर संतानें और रोजमर्रा की खिटखिटें उसे अधिक प्रामाणिक जान पड़ती हैं। अपनी कल्पना में स्त्री स्वयं को एक ही समय निर्वासित करती है और स्थापित भी। कुछ ऐसे कि एक स्त्री के भाग्य में जो कुछ घटता है वह संसार भर की स्त्रियों के भीतरी संसार को प्रभावित करता है। क्या ऐसा कोई दावा हम ‘पुरुष-लेखन’ के लिए कर सकते हैं?
कठिन परिस्थितियों में अर्जित की गई कला, वह एक नीग्रो की हो या यहूदी की, राजनैतिक बंदी की हो या स्त्री की, एक अलग गरिमा लिए रहती है। हमारी औसत गृहस्थियों की घुटन ने हमारी स्त्रियों की कल्पनाशीलता को जो अभूतपूर्व आयाम दिए हैं उसे कौन नहीं जानता। वे हमारे लोक-साहित्य में लोरियाँ हो, विदा-गीत हो, या ससुराल के कुटुंबियों का उपहास – स्त्रियाँ हर हालत में अपने लिए एक झरोखा बना लेती हैं। एक ऐसा आकाश का गीत जिसे सिर्फ पिंजरे में रहने वाला पक्षी ही गा सकता है। यही न केवल उनकी असली स्वतंत्रता है, बल्कि सफलता भी। हालाँकि इस सबका उल्लेख करके मैं किसी भी स्त्री की निजी पीड़ा को छोटा नहीं करना चाहती। यहाँ मेरा अभीष्ट केवल पीड़ा और स्वतंत्रता के रहस्यात्मक संबंध की ओर संकेत करना ही है।
###
तब फिर एक स्त्री का स्वतंत्रता-बोध क्या हो? घर, प्रेम और अपनी जाति से अलग उसकी ऐसी कौन-सी जमीन हो, जो सिर्फ उसकी अपनी हो? क्या यह संभव है कि जिसे हम ‘स्वतंत्रता’ समझते है, वह एक व्यक्ति के जीवन में मूल्य की तरह होती ही न हो? वह केवल उतने ही खंड में घटित होती हो, जितने में उस व्यक्ति-विशेष का रचना-कर्म? कि उसकी रचना-प्रक्रिया अपने लिए कविता के साथ-साथ उतनी भर स्वतंत्रता गढ़ लेती हो, जिसमें कविता साँस ले सके? क्या यह संभव है कि शब्दों के आकाश के अतिरिक्त कविता के पास कोई भी आकाश होता ही न हो? कि कोई दूसरा आकाश स्वयं रचनाकार के पास भी न होता हो? कि इसी कर्ता-कारक के चलते कवि को कविता की, कविता को कवि की जरूरत पड़ती हो – परस्पर मुक्ति के लिए?
एक स्त्री के शब्द ही वह प्रति-संसार हैं जिनमें वह स्वयं को प्रतिष्ठित कर सकती है। एक स्त्री के प्रश्न और संशय ही वह थोड़ी-सी जमीन हैं, जहाँ वह स्वतंत्र है। लिखने के लिए लेकिन जानना जरूरी है। एड्रियन रिच ने कहा भी है :
माना कि तुम लिखना चाहती हो
एक स्त्री दूसरी की
चोटियाँ गूँथ रही हैं, इसके बारे में
सीधी या सलमों-सितारों वाली
तीन वेणियों वाली या खजूरी चोटियाँ
तुम्हें जाननी होगी
बालों की लंबाई, उनका प्रकार
जानना होगा
वह स्त्री क्यों चुन रही है अपनी
चोटियाँ करना
कैसे बनाई जाती हैं वे
किस देश में हो रहा है यह
और क्या-क्या होता है उस मुल्क में
तुम्हें उन सबके बारे में जानना होगा
(नार्थ अमेरिकन टाइम)
लिखने के लिए ‘जानना’ जरूरी है, लेकिन ‘जानने’ के बाद लिखा ही जाए, यह कतई जरूरी नहीं। जानने और अंतिम तौर पर लिखे जाने के बीच ही प्रायः वह आलोक-क्षेत्र रहता है, जहाँ मुक्ति संभव है। जाने हुए सच को लिख देना ही जाने हुए सच से मुक्ति है।
संबंधित पोस्ट:

गगन गिल
गगन गिल (जन्म- 1959, नई दिल्ली) आधुनिक हिन्दी कवियित्रियों में से एक हैं। गगन गिल को 'भारतभूषण अग्रवाल स्मृति पुरस्कार', 'संस्कृति पुरस्कार' और 'केदार सम्मान' से सम्मानित किया जा चुका है।