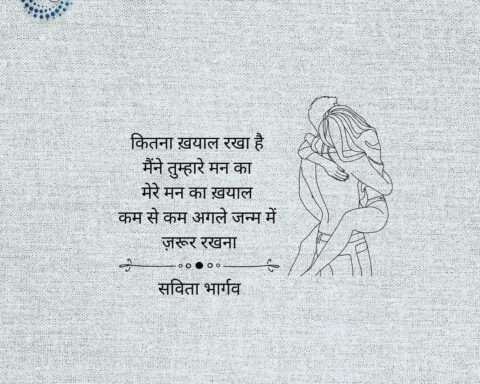बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होय?’ जिसने पहली-पहली बार ऐसा कहा होगा, उसका मन फलों के राजा के रस से आप्लावित रहा होगा।
रहना भी चाहिए। वह कौन है, जिसे फल-राज न पसंद हो। लेकिन बबूल के प्रति उस व्यक्ति के मनोभाव का मैं कभी समर्थक नहीं रहा। माना कि फल और कंटकों के बीच का द्वंद्व कहावत को तीक्ष्णता प्रदान करता है, लेकिन काँटों में बबूल ही क्यों? और भी तो काँटे हैं! ज़्यादा तीखे, ज़्यादा बड़े और ज़्यादा उलझे।
जिसे काँटे गड़े हैं, वह जानता होगा कि बेर के काँटे की तासीर कैसी होती है। गड़ता ही नहीं है, गड़कर फँस जाता है।
माँ कहती है कि एक बार मुझे बेर का काँटा गड़ गया था। एक टाँग पर नाचते घर पहुँचा और घर सर पर उठा लिया। बताती है कि रोता जाऊँ और किसी को हाथ भी न लगाने दूँ। आखिरकार रोते-रोते सो गया, तब जाकर उस कुटिल-कंटक को काढ़ने में किंचित् सफलता मिली। तो यदि काँटे का प्रभाव दिखाना था, तो बेर भी रखा जा सकता था। लेकिन बेर में फल होते हैं। मीठे बेर। शायद इसलिए कहावत में वह कंट्रास पैदा नहीं होता।
काँटे और भी होते हैं और कसम से इतने किस्म-किस्म के होते हैं, कि उनके बीच कुछ चला गया, तो बिना रक्त-दान के फल नहीं मिलेगा। शायद कहनेवाले के दिमाग़ में उनका ख़्याल नहीं आया होगा।
क्या ऐसा हो सकता है कि यह सच की घटना रही हो। यानी बबूल का पेड़ लगाकर कोई आम चाहता रहा हो? कहते हैं कहावतें ऐसे ही अनुभवों से पैदा होती हैं। कहावतों के विषय में यह सामान्य बात भले सही हो, लेकिन इस संदर्भ में मुझे संदेह होता है। कहीं बबूल का पेड़ भी कोई लगाता है?
सचमुच नहीं लगाता है।
किंतु मेरे एक ग्रामीण ने मुझे इस मामले में ग़लत साबित कर दिया। उसने बताया कि उसके एक मेहमान बबूल के फल ले गये ताकि उसे लगा सकें। यह मेरे लिए घोर आश्चर्य की बात थी। ज़्यादा जानने की कोशिश की तो पता लगा, उनके इलाके में यह नहीं मिलता। तब समझ में आया कि यदि न हो तो बबूल जैसों को भी पर्याप्त महत्त्व और सम्मान मिल जाता है। वह एक और कहावत है न- “जहाँ बाग न बगान, वहाँ रेंड़ो परधान।” जब रेंड प्रधान हो सकता है, तो बबूल क्यों नहीं?
भटकने के ख़तरे से खेलते हुए बताना चाहूँगा कि रेंड़ एक पेड़ है, जिसे अरंडी कहा जाता है। उसके फल से तेल निकाला जाता है। मेरे गाँव का नाम रहा- अरण्यडीह। लेकिन मुख-सुख ने इसे अरंडी बना दिया है। मन मुझसे ही सवाल करता है कि क्या तुम्हारा गाँव बे-बाग-बगान इलाक़े में अरंडी की तरह ही प्रधान तो नहीं बना फिरता? यह सवाल मेरे गाँव-वाद को चुनौती है। इसका जवाब मसखरेपन के साथ है कि अब तो वह ‘अरंडी’ भी नहीं बचा, ‘अंडी’ हो गया है। क्या पता एक दिन केवल ‘अ’ ही बचे। अच्छा है, तब कम-से-कम यह तो कह सकूँगा, कि ‘अ’ मेरे गाँव के नाम का संक्षिप्ताक्षर है। पूरा नाम है- अरण्यडीह।
बात कहावत से शुरू हुई थी। मुझे लगता है कि जिसने भी पहले-पहल इसे कहा होगा, उसके सामने अवश्य बबूल बहुतायत में होंगे। क्या पता कोई मेरे ही क्षेत्र का न हो! मेरे आसपास आम कम और बबूल ही अधिक हैं। आम फलता है तो चोर लग जाते हैं, बबूल मंद-मंद हिलता रहता है, हिल-हिल कर बुलाता रहता है और कोई नहीं आता।
बबूल इतना भी उपेक्षणीय नहीं है, जितना कह दिया गया है। गाँवों में अभी भी सुबह-सुबह लोग दातून के लिए बबूल को तकते हैं। वह भी क्या मज़ेदार जीवन होता है कि सुबह-सुबह घर से निकल गए। एक लाठी ले ली। बबूल की कोई पतली-सी टहनी देख भरपूर हाथ लाठी चलाई। दातून मिल गया। दातून में नीम का नाम ज्यादा उज्ज्वल है, लेकिन उसके दातून से जीभी उतनी अच्छी नहीं बनती, जितनी कि बबूल से। कुछ तो गुण अवश्य रहे होंगे कि एक टूथपेस्ट कंपनी ने अपने उत्पाद का नाम इसके नाम से रखा है। बबूल बेचारा पेड़ है, कोई इसपर ध्यान नहीं देता, वर्ना ऐसा भी हो सकता था कि नाम के इस्तेमाल पर कोर्ट तक घसीट देता। एक वैद्यनुमा सज्जन ने बताया था कि बबूल एक औषधीय वृक्ष भी है। इसकी छाल, पत्ती, फल, फूल और गोंद सभी में औषधीय गुण होते हैं। निश्चय ही इसी सुनाम का दोहन वह कंपनी कर रही है। कुदरत ने सबको ‘कुछ-न-कुछ’ बख्शा ही है। मनुष्य है कि उस ‘कुछ-न-कुछ’ का दोहन किये जा रहा है।
अब लकड़ी के हल का जमाना लद गया है। मुझे याद आता है- किसान बबूल के पेड़ को इस नज़र से भी तोलते थे कि यह हल के लायक हो गया है, अथवा इससे कितने हल बन जाएँगे। साफ कहूँ तो बबूल ने अपने को खेत जोतने में लगाया है। हम उस अनाज को खाकर बड़े हुए हैं, जिसके आने में बबूल की कुर्बानी शामिल है। बबूल के हम कर्जदार हैं।
कभी इसे धार्मिक सम्मान भी प्राप्त था। पीपल-बरगद की तरह इसपर भी ईश्वर का वास माना जाता था, लेकिन लगता है ईश्वर इस कँटीले आसन पर देर तक विराजित नहीं रह सके होंगे। आख़िर वे हम जैसे बच्चे तो रहे नहीं होंगे कि कभी गोंद, कभी दातून, तो कभी गिल्ली-डंडा के लिए ही बबूल तक भागे चले आते हों।
शुद्ध उपयोगितावादी होकर भी सोचें तो, पाते हैं कि बबूल का सबसे अधिक उपयोग बाड़ा बनाने में हुआ। बाड़ा रक्षक-शक्ति है। बाड़े में अन्य पौधे सुरक्षित रहते हैं और बढ़ते जाते हैं। कभी किसी बड़े पेड़ ने बाल-रूप को यह अपने कंटकित शरीर से सुरक्षा देता है, तो कभी साग-सब्जी के छोटे पौधों को। कितने रसदार फल इसके ऋणी रहे हैं, इसकी गिनती नहीं है। मैं जब भी किसी बाड़े में झूमते हरे-हरे पौधे को ताकता हूँ, तो एक विडंबना के दर्शन करता हूँ। बताइए तो, किसी हरे को काटकर खड़ा कर दिया गया। वह निरंतर सूखता जाता है और उससे जो रक्षित हैं, वे हरे-भरे होते जाते हैं। किसी के हरेपन में किसी का सूखना शामिल है। ख़ुद सूखकर हरियाली बचा लेना सामान्य काम तो नहीं हो सकता।
एक चैती लोकगीत है। उसमें नायिका न जाने किसलिए बबूल के वन में चली जाती है? उसके पाँव में काँटे चुभ जाते हैं। काँटा तो पैर में चुभता है, लेकिन टीस दिल में उठती है-
कंटवा गड़त, जियरा साले हो रामा
बबूरी के बनमा।
नायिका चिंतित है कि यह काँटा कौन निकालेगा और दर्द कौन हरेगा। यह दर्द तो पिया ही हर सकते हैं-
देवरा निकाले रामा बबूरी के कंटवा हो
पिया मोरा हरतय दरदिया हो रामा…..
बबूल का इतना रोमांटिक उपयोग कोई कवि ही कर सकता है। वह कवि कौन रहा होगा? कहाँ का रहा होगा कवि? निश्चय ही उसके आसपास बबूल का वन रहा होगा। कहीं वह हमारी पहाड़ी की बात तो नहीं कर रहा। इस अर्थं पर मैं जरा देर ही ठहर पाता हूँ। कवियों ने रोमांस के लिए चाहे जिन परिस्थतियों में जगह बना ली हो, लेकिन एक लोक-गीत-कवि क्या इसलिए ही रचता रहा। मुझे लगता है कि इसमें पीड़ा है। काँटा गड़ने से अलग की पीड़ा है। एक काँटा पैर में गड़ा है, तो एक मन में भी गड़ा है। नायिका अवश्य अपने पिया से दूर है, या यूँ कहूँ उसका पिया उससे दूर रह रहा है। एक टीस है कि पिया साथ में होता, तो वह इन कँटीले जंगलों में क्यों फिरती? या ऐसा तो नहीं कि अकेली औरत के लिए पूरा समाज कंटीला हो जाता हो? कहना कठिन है कि बात क्या थी लेकिन जो बात निकलती है, उससे भी तो इनकार नहीं किया जा सकता।
मेरे गाँव के उत्तर में खड़ी पहाड़ी अपने कंटकाकीर्ण होने के लिए भी जानी जाती थी। एक ग्रामीण थे। हर किसी से पूछ्ते थे- ‘पहाड़ गए थे?’ जानेवाले ने ‘हाँ’ कहा, तो अगला सवाल होता- ‘काँटा गड़ा?’ इसका जवाब यदि ‘हाँ’ होता तब तो ठीक था, संतुष्टिदायक। यदि ‘ना’ होता तो वे कह बैठते- ‘कैसे पहाड़ गए थे कि काँटा ही नहीं गड़ा? यानी गए ही नहीं।’
उनके लिए पहाड़ जाने का मतलब काँटों का गड़ना था। न जाने वे किस अर्थ में यह कहते होंगे, लेकिन उनके गुजरने के वर्षों बाद उनका एक वंशज सोच रहा है- ऊँचा जाने के लिए काँटों के बीच से गुजरना ही पड़ता है। ऊपर उठने में गड़ते ही हैं काँटे।
अब पहाड़ तो है, उसपर बबूल नहीं है। बबूल के बिना ही पहाड़ वह उजाड़-उजाड़ लगता है। एक बबूल भी हो तो हरियाली लौट आए। सचमुच पहाड़ सबसे ज्यादा बबूल को ही चाहता होगा। जब पेड़ कटने लगे, तो सबसे पहले इमारती पेड़ कटे, फिर दूसरे पेड़। बबूल तो बाद तक रहे। जिसे जलावन के लिए भी पेड़ से दुश्मनी थी, उन्होंने बबूल काटे। अभी भी उगते हैं तो सबसे पहले बबूल ही। शरीर में काँटों के होने का यह अर्थ कहीं नहीं है कि उसपर विश्वास ही न किया जा सके अथवा वह रिश्ते निभा ही नहीं सकता है। क्या पता वही सबसे ज्यादा रिश्ते निभा लेता हो।
मुझे आभास है। कोई यह सवाल कर सकता है- बबूल भी लेखन का विषय हो सकता है क्या? अरे लिखना ही है, तो आम-अमरूद जैसे फलदार पेड़ को विषय बनाया जाए अथवा पीपल-बरगद जैसे छायादार को। यह क्या कि काँटों पर लिखने के लिए बैठ लिए?
लेकिन मैं क्या करूँ, यदि मेरे आस-पास काँटे-ही-काँटे हों तो? मैं फल-फूल ढूँढने कहाँ जाऊँ? मेरे सामने यही तीखे काँटे हैं। मैं उन पर ही विश्वास क्यों न करूँ? उनकी जीवनी-शक्ति को क्यों न देखूँ? कोई बताये ऐसा पेड़ कोई और है क्या? आज तक इसे किसी ने नहीं लगाया, आज तक इसे किसी ने बचाया नहीं, उगते ही दातून की पहचान कर चोट की गयी तो बढ़ते ही काट लिया गया। इस पर भी बबूल है और खूब है। यह काँटे ही नहीं रखता, बकरियों से पूछो वह बताएगी, इसके पास कोमल पात भी हैं। और यदि सौदर्य-खोजी दृष्टि हो, तब आप इसके फूल को भी पाएँगे। फूल गुलाब(इसे भी काँटों ने कब छोड़ा है) का टक्कर भले न लें, पर ध्यान तो खींच ही लेंगे।
कभी विज्ञान के शिक्षक ने बताया था कि काँटे यूँ ही नहीं हो जाते हैं। यह पेड़ों का अनुकूलन है। ज्यादातर काँटेदार वनस्पति उन जगहों में मिलती है, जहाँ पानी कम होता हो, मसलन रेगिस्तान। पानी के खर्च को कम करने के लिए पेड़ अपनी पत्तियों को छोटा करते चले जाते हैं। ऐसा भी होने लगता है कि पत्तियाँ नए रूप में आने लगें। काँटों के रूप में।
काँटे पत्तियों के बदले रूप होते हैं।
जब भी यह सोचता हूँ, बबूल के प्रति संवेदनासिक्त हो जाता हूँ। आखिर कितना निर्जल रहा होगा कि काँटे उग आए? और कितनी सदियों से पानी के लिए तरसता रहा होगा कि आज मैदानों में भी है, फिर भी न काँटों को छोड़ पाता है और न ही पत्तियों को फैला पाता है? बबूल का काँटेदार होना, उसका दोष नहीं है। यह तो उस वातावरण का दोष है, जो किसी को पानी तक नहीं दे सकता।
आज भी कोई मिलता है, जिसके व्यवहार में काँटे उगे हों, तो मैं यह सोचता हूँ कि ये काँटे कभी हरे-हरे पत्ते रहे होंगे। कोमल और चिकने। यदि इनके साथ उचित व्यवहार हो, तो क्या पता ये फिर से पत्ते हो जाएँ! आखिर जब वातावरण की उपेक्षा से पत्ते काँटों में बदल सकते हैं, तो संवेदनापूर्ण व्यवहार से वे फिर से पत्ते क्यों नहीं हो सकते?
मेरा विश्वास है कि ऐसा होगा ज़रूर। तब एक नया मुहावरा बनेगा- “पुनर्पत्रो भवः।”
सचमुच कितना प्यारा होगा न- काँटों का कोमल पत्ता हो जाना!

अस्मुरारी नंदन मिश्र
अस्मुरारी नंदन मिश्र मौजूदा वक़्त के माने हुए कवि व् प्रतिष्ठि साहित्यकार हैं. आप इन दिनों विदिशा, मध्यप्रदेश में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं. आपकी रचनायें समय-समय पर विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं. इन दिनों आपका पहला काव्य संग्रह 'चांदमारी समय' अपने पाठकों के बीच है.